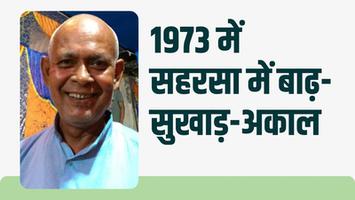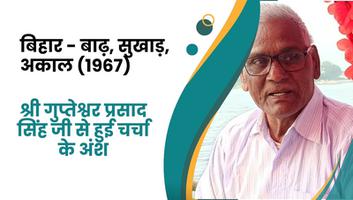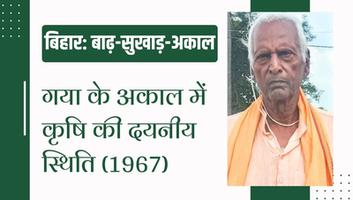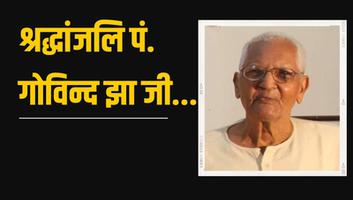कोसी नदी अपडेट - बिहार-बाढ़-सुखाड़-अकाल, जब बाढ़ में तैरते धान ने अकाल को मात दी
- By
- Dr Dinesh kumar Mishra
- September-05-2024
बिहार-बाढ़-सुखाड़-अकाल
गंगा के उत्तरी बिहार में सुखाड़ या अकाल की चर्चा अजीब लग सकती है, क्योंकि यह क्षेत्र सामान्यतः बाढ़ से प्रभावित माना जाता है। फिर भी, इतिहास गवाह है कि यहाँ कभी-कभी भयंकर सुखाड़ ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है। ऐसी ही एक घटना 1972 में पूर्णिया (अब कटिहार) जिले के प्राणपुर प्रखंड के केहुनिया गाँव में घटी थी, जब प्राकृतिक आपदा के दो विरोधी रूप—बाढ़ और सुखाड़—ने एक साथ चुनौती खड़ी की।
श्री शिवदेव झा की स्मृतियाँ: संघर्ष और सहयोग का दौर
70 वर्षीय श्री शिवदेव झा बताते हैं, "1972 में, मैट्रिक की परीक्षा पास करने के बाद मैंने इस इलाके में भयंकर सुखाड़ का सामना किया। धान की खेती छींटा विधि से होती थी, और उपज भी सीमित रहती थी। बाढ़ और सूखा, दोनों ने जीवन को मुश्किल बना दिया था।"
बाढ़ के अनुकूल 'चिन्ताभोग धान'
सुखाड़ के समय भी कुछ उपाय मौजूद थे। चिन्ताभोग धान, जिसे बाढ़ में भी उगाया जा सकता था, इस क्षेत्र की अनूठी विशेषता थी। यह फसल बाढ़ के साथ बढ़ती थी और नाव पर सवार होकर काटी जाती थी। हालांकि उपज कम होती थी, लेकिन यह अनाज संकट के समय ग्रामीणों के लिए राहत का साधन बनता था।
गाँव में उधार की प्रथा
अकाल के समय, ग्रामीणों के बीच धान उधार देने-लेने की प्रथा थी। श्री झा के परिवार की स्थिति बेहतर थी, इसलिए उनके पिता जरूरतमंदों को धान उधार देते थे। शर्त बस इतनी होती थी कि अगहनी फसल के बाद इसे लौटा दिया जाए। अधिकांश लोग समय पर उधार लौटाते थे, लेकिन कुछ को अतिरिक्त मोहलत भी मिलती थी।
लूट-पाट की घटना
श्री झा याद करते हैं कि उनके गाँव के झरना टोला में पूरन साह जी के यहाँ लूट-पाट हुई थी। यह घटना उस कठिन समय की गंभीरता को दिखाती है, जब बाढ़ और सुखाड़ के बीच जीवन और संसाधनों की सुरक्षा कठिन हो जाती थी।
प्राकृतिक आपदा और सामुदायिक सहयोग
1972 का यह दौर बिहार के ग्रामीण समाज में सामुदायिक सहयोग और संघर्ष की मिसाल है। बाढ़ और सुखाड़ जैसे विपरीत संकटों के बावजूद, ग्रामीणों ने एक-दूसरे की मदद से मुश्किल हालात का सामना किया। श्री शिवदेव झा की स्मृतियाँ यह बताती हैं कि कैसे संघर्ष, सहानुभूति और सहयोग के जरिए संकट के दिनों को पार किया गया।
क्रमशः
(अगले अंश में जानेंगे, कैसे प्राकृतिक आपदाओं ने बिहार की खेती और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया।)