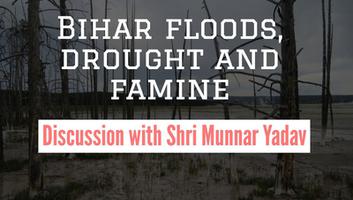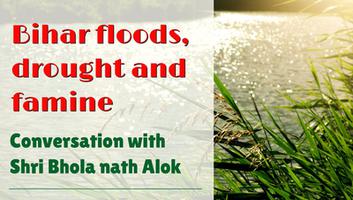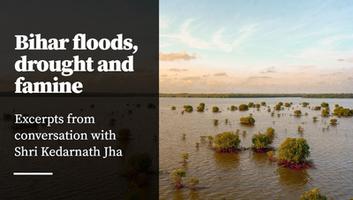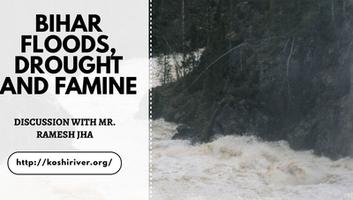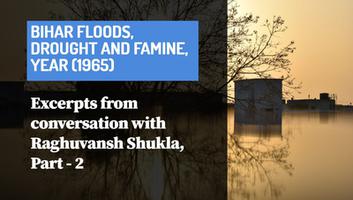कोसी नदी अपडेट - पंडित गोविन्द झा से कोसी-कमला बाढ़ के विषय में हुयी वार्ता के अंश
- By
- Dr Dinesh kumar Mishra
- October-12-2019
पंडित गोविन्द झा, मूल गाँव इसह्पुर, पोस्ट सरिसब पाही, जिला मधुबनी से कोसी-कमला की बाढ़ के बारे में हुई मेरी उनसे बातचीत के अंश. 99 वर्षीय पंडित झा आजकल पटना में पटेल नगर में रहते हैं। उन्होनें मुझे बताया कि,
"तब बाढ़ कोई विभीषिका नहीं थी. 1954 में कमला मधुबनी के पूरब में आ गई थी और तब हम लोगों को काफी कठिनाई का सामना करना पडा था. पर साधारणतः नदी की बाढ़ से हम लोगों को कोई परेशानी नहीं थी. फूस के घर थे और उनमें पानी भर भी जाए तो तो लोग उसके छप्पर पर चले जाते थे, यह लगभग हर साल का किस्सा था इसलिए तैयारी रहती थी. घर दुबारा भी बनाना पड़ जाए तो भी आसमान नहीं टूटता था. बाढ़ का ठहराव बहुत कम होता था, ज्यादा से ज्यादा सात दिन और उसके अनुरूप जलावन, साग-सब्जी आदि की व्यवस्था कर ली जाती थी. पानी आता था तो मछली वरदान बन कर खुद-ब-खुद आ जाती थी. हमारे गाँव में आठ पोखरे थे. हर बड़े आदमी के पास पोखरे थे.
बाढ़ में मछली अंडा छोड़ती थी, अंडे बिखर जाते थे और बाढ़ में हर जगह मछली पहुँच जाती थे. सड़क पर भी मछली आ जाती थी. सबको उपलब्ध थी. खेत में नया बालू और मिटटी पड़ती थी. बालू वाले खेत में ककड़ी आदि होती थी और मिटटी वाले खेत में धान जबरदस्त होता था. बीमारी जरूर बहुत आती थी. मलेरिया, कालाजार फैलता था, लोग मरते भी थे. पानी दूषित हो जाता था. उसके चलते परेशानी होती थी. इससे भी बीमारी फैलती है.
कमला जब 1954 में मधुबनी के पूरब आ गई तब मधुबनी वाले बहुत चिंतित हुए कि कमला क्यों उधर चली गई? यहाँ के राजा रामेश्वर सिंह बहुत पूजा पाठ करने वाले थे और वो एक बार आसन लगा कर ध्यान लेकर बैठ गए कि कमला वापस अपने स्थान पर चली आये. लेकिन पुरानी कमला सूखती गई और घुटने भर पानी में ही दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन करना पड़ता था. बहुत से पेड़ सूख गए.
मैं कुछ दिन लालपुर सुरहोपट्टी, सिंघेश्वर स्थान के पांच-सात किलोमीटर उत्तर-पूरब में पढ़ाने के लिए गया था. वहाँ कोई पेड़ पौधा नहीं था. लोग धान की जड़ से दातुन करते थे. सिर्फ पटुआ ही दिखाई पड़ता था. अनाज का कोई निशान नहीं था, केवल बालू था और बालू का ही व्यापार वहां होता था क्योंकि वह बालू भवन निर्माण में सोन नदी के बालू का मुकाबला करता था. यह क्षेत्र ललित नारायण मिश्र के गाँव तक फैला हुआ था. मुमकिन है कि इसीलिये उनके गाँव का नाम बलुआ बाज़ार पडा हो.
यह बालू तीन किस्म का होता था. पहला वो जिसमें कण मोटे थे और उसका उपयोग भवन निर्माण में होता था. दूसरा वो जिसमे बालू बहुत महीन था और उसमे मिटटी मिली हुई थी. ऐसा बालू जिस जमीन पर पड़ गया वह तो धन्य हो गया मगर जिसके खेत पर बालू के बीच वाले कण पड़े और जिसमें लेश मात्र भी मिटटी नहीं थी वह बरबाद हो गया. यही बीच वाला जो बालू था, जिसका कोई उपयोग नहीं था, वह नदी की पेटी में बैठता गया और उसे ऊपर उठाता गया. यह काम कोसी में ही नहीं, हमारी कमला में भी हो रहा था. नदियों के पानी के रास्ते में जब रुकावट डाली जाने लगी, वह चाहे प्राकृतिक तौर पर बालू जमने से हुआ हो या तटबंधों के निर्माण के कारण हुआ हो, परेशानी बढ़ती गई. नदी की पेटी में बालू भरने से नदी का क्षरण हुआ और बाढ़ ज्यादा दिन टिकने लगी. जो बाढ़ तीन से सात दिन में उतर जाती थी अब वह स्थायी होने लगी. बाढ़ का स्वरुप भयानक होता गया.मेरे गाँव के पश्चिम में कभी कमला बहती थी और उसका पाट बड़ा हुआ करता था. इस नदी को इतिहासकार माहिष्मती कहते थे. यह सकरी से होकर बहती थी.
"मैंने कुछ वर्ष नेपाल में जलेश्वर के उत्तर पूर्व में बिताये हैं. यह जगह सुरसंड से पूरब पड़ती है. वहाँ नदी का अद्भुत रंग देखा. वहाँ यह रिवाज़ था कि जैसे ही नदी में पानी आता था तो स्थानीय किसान उस पानी को बाँध कर नदी के पानी को अपने खेतों में ले जाते थे. पानी के रोक दिए जाने के फलस्वरूप नीचे के इलाकों में त्राहि-त्राहि मचती थी कि पानी छोडो, पानी छोडो. कभी कभी झगड़ा भी हो जाता था. लेकिन उनकी यह सिंचाई व्यवस्था काम करती थी. अब वहाँ क्या हाल है वह तो मैं नहीं जानता. मैं जहां रहता था उसके 1-2 किलोमीटर की दूरी पर फुलावामा में हाट लगती थी और हमारी सारी रसद वहीं से आती थी. बीच में एक धार पड़ती थी जिसे तैर कर पार करना पड़ता था और फिर एक काठ का पुल था उसे पार करना पड़ता था. तैर करके नदी पार करना एक आम बात थी. बरसात के बाद नदी आसपास की नीची जमीन को पानी से भर देती थी और यह पानी लगभग स्थिर रहता था, कभी कभी बहता भी था. हमारे यहाँ जो काम तालाब करते थे वही काम नेपाल के इस हिस्से में ये मोइन करते थे."