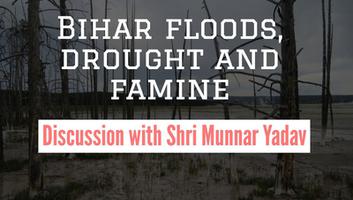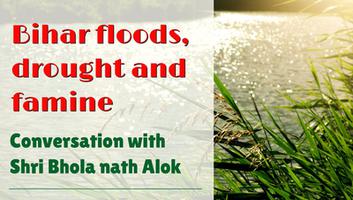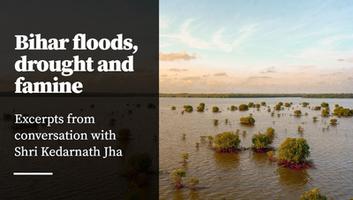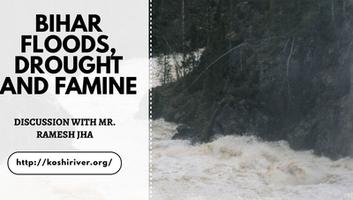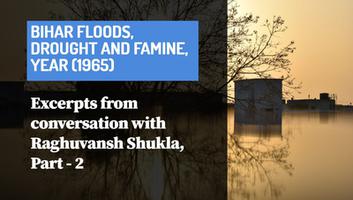आज़ादी के बाद बिहार में बाढ़, सुखाड़ का मूल तलाश करने के क्रम में हाल में मेरी मुलाकात 90 वर्षीय जमशेदपुर निवासी श्री हरि बल्लभ सिंह ‘आरसी’ जी, ग्राम – मधेपुर चंदेल, प्रखंड भगवान पुर, जिला – (उस समय मुंगेर, वर्तमान बेगूसराय) से हुई। उन्होंने मेरा ज्ञानवर्धन इन शब्दों में किया।
मैं तो मूलतः बेगूसराय का बाशिंदा हूँ. बरौनी, तेघरा, बछवारा, समस्तीपुर आदि हमारा कार्यक्षेत्र रहा है. गंगा का पुल हमारे सामने बना है. उसके पहले गंगा को नाव या स्टीमर से पार करना पड़ता था. दो घंटे तक का समय लग जाता था. अब तो पुल बन जाने के बाद 8-10 मिनट में यह यात्रा तय हो जाती है.
मैं जब पहली बार 1950 के दशक के मध्य में जमशेदपुर आया था तो नाव से ही गंगा पार कर के आया था और जब यहाँ से कुछ साल बाद वापस गया तब पुल बन चुका था. पुल बन जाने से गंगा के कटाव में कोई परिवर्तन आया यह मेरे लिए कह पाना मुश्किल है क्योंकि लगभग तबसे मैं जमशेदपुर में ही हूँ. फिर भी गंगा के दाहिने किनारे की मुंगेर की तरफ की मिटटी काली है और मजबूत है जबकि गंगा के उत्तर वाली ज़मीन बलुआही है और नदी उसे आसानी से काट सकती है. बेगूसराय से पूरब रहीमपुर का दियारा का इलाका कटाव से हर साल बरबाद होता है. उधर खगड़िया और बेगुसराय के कितने गाँवों को गंगा ने अपने में समेट लिया है.
पहले गाँवों में तालाब, पोखर, कुएं, बहुत हुआ करते थे. बहुत जगह नदियाँ, आहर और पइन भी थे. धीरे-धीरे उनका उपयोग कम होता गया और उनकी जगह आधुनिक तरीकों ने ले ली. यह बात ध्यान देने की है कि समूचे बिहार में एक साथ कभी भी सूखा नहीं पड़ा है और न कभी एक साथ बाढ़ ही आयी है. यह सब कभी यहाँ, कभी वहाँ, कभी इस साल तो कभी उस साल तो कभी दो चार जिलों में एक साथ हो गया तो हो गया.
यह घटनाएं कभी उत्तर बिहार में तो कभी दक्षिण बिहार में तो कभी पूरब या कभी पश्चिम में होती रही हैं. जहां सूखा पड़ गया, वहाँ अनाज घट जाएगा तो उसे बाहर से मंगवाना पड़ेगा, यह तय है. यह बाहर से अनाज लाने वाले लोग या एजेंसियां कौन सी थीं, यह जानना जरूरी है. आज़ादी के बाद के दिनों में इनमें से बड़ी मात्रा में शासक दल के लोग और उनके कार्यकर्ता शामिल थे जिन्हें प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सत्ताधारी दल का समर्थन प्राप्त था.
तब राशन के वितरण में गड़बड़ियां हुआ करती थीं और कालाबाजारी की भी शिकायतें आती थीं यहाँ तक कि केरोसीन के तेल का भी ब्लैक होता था, केरोसीन का इस्तेमाल ढिबरियों और लालटेन में होता था, न मिले तो घर में अन्धेरा ही रहेगा. खेती करने के लिए तब ब्लाक से ऋण दिया जाता था और बी.डी.ओ. खेतों का मुआयना करने जाते थे. अच्छी फसल होने पर पुरस्कार की भी व्यवस्था थी. यह सब कार्यक्रम अच्छे थे मगर पार्टी कार्यकर्ताओं की अपनी दृष्टि थी. मजदूरों की मजदूरी की दर काफी कम थी और किसान अमूमन मजदूरी का भुगतान अनाज की शक्ल में ही किया करते थे. यह अनाज आमतौर पर वह अनाज होता था जो किसान खुद उपयोग में नहीं लाते थे. इस स्थिति को अच्छा तो नहीं कहा जा सकता था पर यह भुखमरी से बचाव कर ले जाता था.
1950 और उसके बाद के कुछ वर्षों में जब लगातार फसल मारी गयी तब सरकार को अनाज का प्रबंध करना पडा. उस वक़्त देश के कई अन्य राज्यों में खाद्यान्न का उत्पादन कम हुआ था और अनाज विदेशों से मंगवाना पड़ गया था. इसके पहले यह जरूरी था कि स्थानीय स्तर पर बड़े किसानों से कहा जाये कि वह अपना जरूरत से फाजिल अनाज सरकार को बेच दें. अनाज की कीमत सरकार ही तय करती थी। खेतों की पैदावार देख कर सरकार यह भी तय करती थी कि किस किसान को कितना अनाज सरकार को देना पड़ेगा.
किसान को बाज़ार में अपने अनाज की ज्यादा कीमत मिलती थी और वैसे भी फसल काटने के पहले अगर कोई आदमी किसी किसान से एक सेर अनाज उधार लेता था तो उसे फसल काटने के बाद सवा सेर अनाज किसान को देना पड़ता था. यह दोनों ही तरीके किसान के हक़ में जाते थे और वह सरकार की जो लेवी लगाने की व्यवस्था थी उसमें अनाज देने से कतराते थे. अनाज उगाहने के लिए सरकार को लेवी लगाने की जरूरत पड़ती थी और किसान को उससे बचने का प्रयास करना पड़ता था जो उसके हिसाब से वाजिब था. लेवी का झगड़ा यही था. जो चालू व्यवस्था थी उसमें कोई भूखों नहीं मरता था क्योंकि बाहर चाहे जितनी भी कमी रहती हो गाँव के अन्दर अनाज की कभी कमी नहीं होती थी.
दुर्भाग्य यह हुआ कि आज़ादी के बाद हमारे जो कार्यकर्ता थे उनमें ईमानदारी की कमी थी. अगर उसी समय ईमानदारी से काम हुआ होता तो वही हमारा संस्कार बन जाता. जब से कालाबाजारी, जमाखोरी और अपने लोगों को आगे बढ़ाने का काम शुरू हुआ तभी से हमारा संस्कार गड़बड़ा गया और पतन शुरू हुआ. उस समय जब अकाल की स्थिति बनी तब लोगों को रोज़गार देने के लिए हमारे यहाँ बेगूसराय में एक बाँध बनाने की स्कीम आई. इसमें नदी के किनारे एक बाढ़ रोधी बाँध बनाने की बात थी और यह काम मुखिया जी के पास आया. मुखिया जी और बी.डी.ओ. की सहमति से यह काम ठेकेदार को दिया जाना था. उस समय जो मुंगेर के कलक्टर थे, उनकी रुचि बेगूसराय के एक बहुत बड़े प्रभावशाली आदमी के भाई, जो खुद एक बहुत बड़े वकील थे, को यह ठेका देने में थी.
कलक्टर ने बी.डी.ओ. पर दबाव डाल कर इस काम का ठेका वकील साहब को दिलवा दिया. हम लोग उस समय भारत सेवक समाज के कार्यकर्ता थे और हम लोगों ने तय किया कि यह काम अगर वकील साहब को मिल गया तब यहाँ के गरीब मजदूरों का क्या होगा? हम लोगों ने समाज के अधिकारियों को सूचित करके सारी स्थिति को स्पष्ट किया. बिहार के प्रांत प्रभारी स्वामी हरिनारायणानन्द को भी लिखा गया. स्वामी जी भी उन दिनों बहुत प्रभावशाली आदमी थे. उन्होनें बी.डी.ओ. को लिख कर उस ठेके को निरस्त करवा दिया.
बैजनाथ चौधरी भी बेगूसराय के बहुत ही स्वनामधन्य नेता थे और समाज में उनकी बहुत धाक थी. उनके साथ मिल कर हम लोगों ने राज्य में एक पुस्तकालय आन्दोलन चलाया था. गाँवों में जाकर पुस्तकालय शुरू करना हमारा काम था. तब सरकार भी इसमें, छोटा ही सही, भवन बनाने में मदद की थी और किताबों की भी मदद की थी. लोग पढ़ने आते भी थे. धीरे-धीरे पढ़ाई में रुचि कम होते-होते प्रायः ख़त्म हो गयी और ग्रामीण पुस्तकालय वहीं बचे हैं जहां ग्रामीणों ने उन्हें बचाने में रुचि ली है.