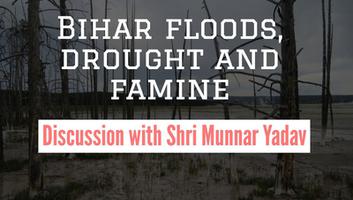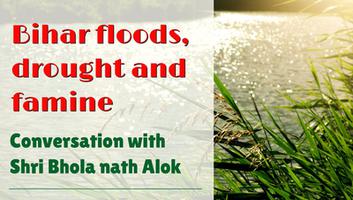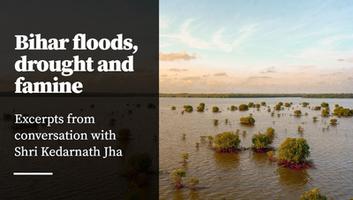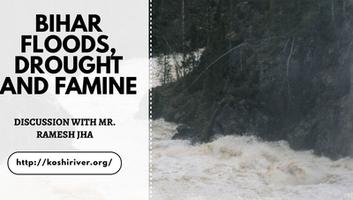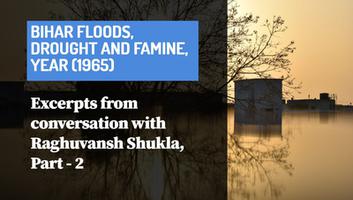कोसी नदी अपडेट - बिहार बाढ़, सुखाड़ और अकाल सीरीज, श्री ऋषिकेश सिंह से हुयी बातचीत के अंश
- By
- Dr Dinesh kumar Mishra
- March-17-2020
श्री ऋषिकेश सिंह (86), ग्राम/पोस्टर रामपुर गंगौली, जिला सीतामढ़ी से हुई मेरी बातचीत के कुछ अंश.
गाँव के श्मशान में तो पानी भरा हुआ था तो कहाँ मुर्दा जलाते?
1954 में मैं 20 साल का रहा होऊंगा. उस साल हमारा घर छोड़ करके गाँव के हर घर में बागमती का पानी घुसा हुआ था. बड़ी संख्या में घर गिरे थे और सारे रास्ते डूबे हुए थे. यह पानी एक सप्ताह तक गाँव में रहा जिसकी वजह से भदई और अगहनी धान – सब बह गया था. कच्चे मकान बहुत गिरे थे जिनको फिर से बनाने के लिए सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिली थी. खाने का सामान भी कुछ नहीं मिला था. सरकार के केन्द्रों से कुछ अनाज मिल जाता था पर वहां जाना पड़ता था. जिसको जरूरत होती थी और रास्ते में अगर पानी न हो तो वह वहां से ले सकता था. बाढ़ पीड़ितों को मदद की जरूरत उन दिनों भी थी मगर आज की तरह हल्ला करना कोई नहीं जानता था.
मेरे बाबा दो भाई थे और हमारा घर 22 कमरे का था. दोनों बाबा लोगों के हिस्से में ग्यारह-ग्यारह कमरे थे. अकेला पक्का मकान था इलाके में. इसके बाद पक्का मकान सिर्फ खैरवा में था और उसके बाद फिर सीधे सीतामढ़ी. बाढ़ के समय बहुत से गाँव के लोग शरण लेने के लिए हमारे घर आ गए थे. ऊपर लोग खाना बनाते थे और सामूहिक भोज होता था. कुछ लोग चूड़ा-दही खाते थे.
हमारे घर में पुआल के आठ विशाल टाल थे जिसमें से जिसको जितना चाहिए खींच ले जाता था. दूसरे लोगों के भी ऐसे ही टाल थे इसलिए गाँव में चारे की कोई कमी नहीं थी. उन दिनों सारा धान खलिहान में इकट्ठा होता था और वहीं दौनी होती थी. अब तो ना जाने कितने किस्म के धान आ गए हैं और भादों में ही दौनी शुरू हो जाती है. अब खलिहान ख़त्म हो गए हैं और खेत में दौनी हो जाती है.
मजदूरों को बड़े किसान पोस कर रखते थे और उनके सुख-दुःख का ख्याल रखते थे क्योंकि उनके बिना उनका भी काम नहीं चलता था. जरूरत के समय किसान अपनी बहेड़ी (अनाज रखने की बड़ी कोठी) खोल देते थे. एक-एक बहेड़ी में 2-2 हजार मन धान आ जाता था. साधारण कोठी में हज़ार मन धान आ जाता था. कभी अकाल पड़ ही गया तो उसका असर बड़े लोगों पर थोड़े ही पड़ता था और छोटे लोग अगर परेशान होते थे तो उनको गाँव का संरक्षण प्राप्त था. गाँव पर अकाल का असर नहीं पड़ने दिया जाता था.
कंट्रोल में कुछ कपड़ा आता था और कपडे की कमी थी. लेकिन उस समय लोग इतना फैशन नहीं करते थे. पीली साड़ी या पीली धोती पहन कर शादी हो जाती थी. न तो आज जैसा दहेज़ था और न दिखावे पर उतना कोई खर्च करता था. अपनी धोती खुद धोकर और पहन कर लोग द्वारपूजा में खड़े हो जाते थे. देखने में नहीं लगता था कि कोई कितना धनी है. अब तो कपडे पर कपड़ा चढ़ता है. दूल्हा खुली पालकी पर आता था तो दुल्हन खड़खड़िया पर आती थी जो हर तरफ से ढकी रहती थी. बस, हो गयी शादी.
1954 में जो बाढ़ आयी थी वह हथिया की वर्षा के पहले आई थी, हथिया में उस साल पानी नहीं हुआ था और एक तरह से सूखा पड़ गया था. हमारे यहाँ अगर बागमती में पानी कम आये या बाढ़ न आये तो वैसे भी सूखा पड़ जाता है पर बागमती की पांक इतनी मजबूत है कि उपज पर सूखे का कोई ख़ास असर नहीं पड़ता. उन दिनों धान काट कर खेत ही में पसार दिया जाता था जिसे पसही कहते थे. धान सूख जाने के बाद मजदूर उसकी अंठी बना कर खलिहान ले जाते थे जहां उसकी दौनी होती थी. अंठी कितनी बड़ी बनेगी यह ले जाने वाले की क्षमता पर निर्भर करता था. सोलह अंठी पर एक अंठी मजदूरी दी जाती थी. मजदूर अपनी अंठी बड़ी बनाता था और खेत से खलिहान तक धान ले जाने के रास्ते में वह पौधों से भी धान सुरुक लेता था, यह सारी बातें हम लोगों को मालूम थी मगर कोई ध्यान नहीं देता था.
दौनी या तो बैलों द्वारा या फिर धान को पीट कर होती थी. रब्बी में छींट देने से खेसारी हो जाती थी और उसी के साथ तीसी और राई हो जाती थी. सरसों का हमारे यहाँ बहुत रिवाज़ नहीं था.
अब बागमती भाग कर पश्चिम शिवहर चली गयी है तो यहाँ बाढ़ आना बंद हो गया है. बाढ़ के समय तीन-चार आदमी हमारे गाँव में मर गए थे, उनको जलाने के लिए गाँव में सूखी जगह नहीं थी. सामने सड़क को ऊंचा करने के लिए मिट्टी रखी हुई थी. उसी डीह पर लाश रख कर उसे जलाना पड़ा था. गाँव के श्मशान में तो पानी भरा हुआ था तो कहाँ मुर्दा जलाते?
श्री ऋषिकेश सिंह