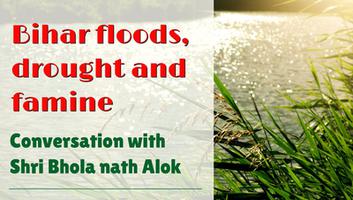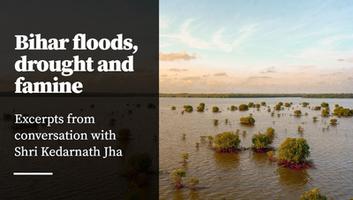कोसी नदी अपडेट - बिहार में बाढ़, सुखाड़ और अकाल, डॉ. रामदेव झा से हुयी बातचीत के अंश
- By
- Dr Dinesh kumar Mishra
- February-21-2020
86 वर्षीय डॉ. रामदेव झा, ग्राम कबिलपुर, पोस्ट: लहेरियासराय, जिला दरभंगा से हुई मेरी बातचीत के कुछ अंश
1950 में पहले तो बाढ़ आई थी पर उसके बाद सूखा पड़ गया और यह लम्बे समय तक बना रहा. सत्तावन में भी भयंकर सूखा पडा था. सूखा और बाढ़ मिथिला की बहुत बड़ी आपदा है. अकाल ने दस्तक तो मिथिला में 1946 में ही दे दी थी. पंडित चन्द्रनाथ मिश्र अमर की एक रचना है ‘अल्हुआष्टक’ जिसमें अल्हुआ (शकरकंद) की अच्छी प्रशंसा की गई है और उसे पतराखन (इज्ज़त बचाने वाला खाद्य) कहा गया है. सूखा पड़ जाने पर अल्हुआ ही लोगों की जान बचाता था. यह बात अलग है कि उसे वह सम्मान नहीं मिलता था जिसका वह हकदार था क्योंकि परम्परा के अनुसार यह गरीबों का भोजन माना जाता था. आपातस्थिति में उसे सभी खाते थे मगर यह बात स्वीकार नहीं करते थे. जब भी कभी सूखा पड़ता था तब लोग अल्हुआ की फसल पर निर्भर करते थे.
वही अल्हुआ अब दुर्लभ हो गया है और देवोत्थान एकादशी के समय 60-60 रुपये किलो बिकता है. पूजा-पाठ तक के लिए अल्हुआ नहीं मिल पाता है. हमारे यहाँ इसकी खेती साल में दो बार होती थी. एक बार तो इसे कार्तिक मास में बोया जाता था और माघ में खोद कर निकाल लिया जाता था और दूसरी बार माघ में बोते थे और वैशाख मास में निकाल लेते थे. पहले वाले को माघा और दूसरे वाले को बैसाखा कहते थे. गरीबों के लिए तो यह भोजन था ही, अमीरों के लिए यह खाद्य-बीमे का काम करता था.
मड़ुआ हमारे यहां होता था पर इसको भी निम्न स्तरीय अन्न माना जाता था। इसका उपयोग भी गरीब वर्ग के लोग अधिक करते थे.
1950-52 के बीच जो भी होना था वह तो हुआ ही, सूखा राहत हमारे यहाँ 1957 तक बंटी थी. राहत सामग्री के तौर पर हमारे यहाँ गेंहू, मकई, और जनेर मिलता था. कभी कभी बाजरा भी मिलता था जिसे मिथिला के लोग जानते भी नहीं थे. बाक़ी दो चीज़ें भी बहुत प्रचलित नहीं थीं. जनेर की खेती हमारे यहाँ नहीं होती थी. उसे धान के खेत में छींट दिया जाता था और वह घास की तरह उगता था. उसका दाना हमारे यहाँ जानवरों को खिलाया जाता था जो अकाल में हम लोगों को भी खाना पड़ गया था. दो तरह का जनेर सरकार की तरफ से मंगाया जाता था, एक लाल और दूसरा सफ़ेद.
वितरण के लिए कुछ गेंहूँ भी आया था मगर जिसकी समाज में थोड़ी भी हैसियत थी और प्रतिष्ठित लोग कभी भी, राहत सामग्री लेने के लिए नहीं गए. घर में भले ही अन्न कम हो या नहीं भी हो तब भी वह लोग खैरात नहीं लेते थे. खैरात लेना मानहानि का सबब माना जाता था. गरीब लोग मजबूर थे उनके पास राहत लेने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था.
कपडे की हालत तो 1946 से ही बेकाबू थी. पांच गज की धोती और छ: गज की साड़ी का परमिट दिया जाता था. हमारे पिताजी कहीं से एक परमिट लेकर आये थे मगर उस कपडे को लाने के लिए 6 मील दूर जाना पडा था. लहेरियासराय के पास पिड़री घाट और छपराह घाट जैसी जगहें हैं. वहीं की दुकान से कपड़ा मिलता था. वह भी कोरा और मोटा कपड़ा होता था मारकीन का जिसे ननकिलाट कहते थे. यह वास्तव में नॉनग्लेज़्ड कपड़ा था जिसका अपभ्रंश ननकिलाट था. इस कपडे को किसी ऐसे पदार्थ में डुबो देते थे जिससे वह मोटा और खुरदुरा हो जाता था. महिलाएं भी वही कपड़ा पहनने को बाध्य थीं.
कपडे के लिए शादी-ब्याह में भारी दिक्कत आती थी, शौक़ीन और महीन कपडे खरीदने में कोई ख़ास दिक्कत नहीं थी, उसे खरीदने वाले अभिजात्य वर्ग के लोग थे और उनकी दुकानें भी अलग थीं. लहेरियासराय में एक थानमल-पाली राम की दूकान थी जहां महीन कपडे मिलते थे. बाद में उस चौक का नाम ही पालीराम चौक पड़ गया था. यह जगह आज भी उसी नाम से आबाद है. थानमल बाप थे और पालीराम बेटे. आजकल उनका कारोबार उनके पोते-पडपोते संभालते हैं.
महंगाई का आलम यह था कि हमारे स्थानीय कवि महाबीर पासवान ने एक गाना लिखा था कि, “एक पाई में टी ड़ी ड़ी ड़ी, दुई पाई में तीन टा बीड़ी, चार पाई में भेंटै छै सलैया हो जवाहर भैया.” इस तरह के बहुत से गाने उन दिनों लोगों की जबान पर रहते थे।
उपज उन वर्षों में हुई नहीं थी, पैसा किसी के पास था नहीं तो ऐसे बहुत से गाने बड़े प्रसिद्ध हुए थे. एक आना जिसके पास हो गया उसका चार दिन के भोजन का प्रबंध हो जाता था. हम लोग तो बच्चे थे, उतना बोध नहीं था पर यह सब हम लोगों ने भोगा था सो अभी तक याद है.
डॉ. राम देव झा