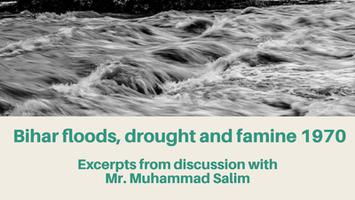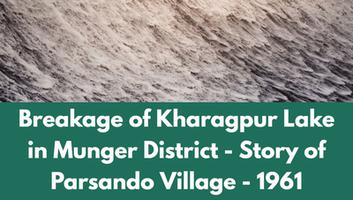कोसी नदी अपडेट - बिहार बाढ़, सुखाड़ और अकाल, श्री कुमार शचीन्द्र सिंह से हुई चर्चा के अंश
- By
- Dr Dinesh kumar Mishra
- May-14-2023
बिहार -बाढ़-सुखाड़ -अकाल
बीरपुर-सुपौल के 91 वर्षीय श्री कुमार शचीन्द्र सिंह से हुई मेरी बातचीत के कुछ अंश
हमारा मूल गाँव आज के समस्तीपुर जिले में डुमरी दियारे में है, जहाँ धान नहीं होता था। हमारे पिताजी खेती, जमीन-जायदाद के बड़े शौकीन थे। धान न होने से हमें चावल खरीद कर खाना पड़ता था और आसपास के लोग ताने मारते थे कि जो खरीद के चावल खाए वो रईस कैसा? तब पिताजी ने मधेपुरा के पास एक अराड़घाट है, वहाँ दरभंगा महाराज से कुछ जमीन बन्दोबस्ती करवा ली जिससे वहाँ धान बोया जा सके। दस साल खेती हुई, उसके बाद कोसी ने उस जमीन को बालू से पाट दिया। जमीन ऊँची हो गयी और धान की खेती फिर बन्द हो गयी।
तब सवाल उठा कि कहाँ जमीन ली जाये, तो पूर्णिया में झलारी नाम की एक जगह है, उसका पता लगा। जहाँ के एक ज़मींदार की जमीन सहरसा के बीरपुर में थी। वह जमीन पिताजी ने बिना देखे खरीद ली।
वहाँ जाने का रास्ता नहीं था। फारबिसगंज रेलगाड़ी से उतर कर 28 मील पैदल चल कर बीरपुर जाना पड़ता था। हमारे यहाँ से कानपुर-जोगबनी ट्रेन चलती थी, जिससे हम लोग पटोरी में बैठते थे और बारह घंटे बाद जोगबनी में उतर जाते थे। वहाँ से आगे जाने के लिए रास्ता केवल पैदल का था। दिन का खाना घर पर ही होता था क्योंकि उन दिनों बाहर कुछ खाने का रिवाज नहीं था। अब घर पहुंचने में चाहे जितना समय लग जाये। इन दिनों बीरपुर में जहाँ अस्पताल है कोसी वहीं से बहा करती थी। भीमनगर नदी के पश्चिम में था, जहाँ हफ्ते में दो दिन हाट लगा करती थी। कोई सामान घट जाये तो लेने के लिये बीरपुर ही जाना पड़ता था और वहाँ जाने के लिये डोंगी वाली नाव से नदी को पार करना पड़ता था। नाव भी कैसी? पेड़ के तने को काट कर उसे खुरच कर डोंगी की शक्ल देते थे जिसके खुलने का कोई समय नहीं होता था। किसान और घसियारे इसी डोंगी से अपना सामान लेकर इस पार से उस पार ले जाया करते थे। इन लोगों के भी खाने पीने का कोई ठिकाना नहीं रहता था। गाय-भैंस का दूध पीते थे लेकिन सीधा दूध भी कहाँ तक पीते? गाय का गोबर जला कर जो कंडा बनता था उसकी राख को दूध में थोड़ा सा डाल कर उसे गाढ़ा करते थे और वही उनका भोजन होता था।
बाजार या आबादी थी ही नहीं। बड़ा संभाल कर खर्च चलाना पड़ता था। दो हाटों के दिनों के बीच आपके यहाँ अगर कोई मेहमान आ गया और दो दिन रह गया तो आपका तो दो दिन का भोजन घट जायेगा। धान तो होता नहीं था, पाट होता था। चावल तो बाहर से ही आने वाला था। बांध का काम जब शुरू हुआ तब उसी साल बाढ़ आयी। बाढ़ से फायदा भी था और नुकसान भी था। फायदा यह था कि जमीन की उर्वरा शक्ति बढ़ती थी पर जब खेती करनी ही नहीं हो तो उर्वरा शक्ति बढ़े या घटे क्या फर्क पड़ता है?
दूध का थोड़ा बहुत कारोबार कर लेना और गाय का बाछा- बाछी बेच लेना, बस यही व्यवसाय था। अनाज के नाम पर मड़ुआ होता था। अकाल पड़ने का मुख्य कारण था कि वहाँ के लोगों ने अपनी जरूरत के हिसाब से अपने को ढाल लिया था। कुछ न मिले तो दूध से काम चलाओ और अल्हुआ उबाल कर रख लो और खा लो। करमी का साग मिलता था, उस से काम चला लिया। मर्द लोग कमर में पटुआ की रस्सी बांध कर आधी धोती लपेट लिया करते थे तो उनका काम चल गया और औरतें मारकीन इन की साड़ी पहन लेती थीं। ब्लाउज पहनने का रिवाज ही नहीं था।
1950-52 में तो यहाँ सिंचाई की कोई सुविधा नहीं थी, खेती भी नहीं होती थी। बीरपुर का तो कहीं से कोई सम्पर्क ही नहीं था। न पूर्णिया से, न सहरसा या सुपौल से, और न ही फारबिसगंज से। जहाँ भी जाना हो वहाँ पैदल ही जाना था। जब सूखा पड़ गया तब हाहाकार मचा। जब यहाँ कोई रहता ही नहीं था तब राहत कार्य किसके लिए किया जाता? कपड़े का जरूर अभाव था। कपड़ा जो भी आता था रिलीफ फंड में उसे स्थानीय नेता लोग जिनके बीच चाहते थे उनके बीच बटवा देते थे। कोई पूछने वाला तो था नहीं। एकछत्र राज्य था उनका। इस क्षेत्र में सरकार की कोई दुकान भी नहीं थी क्योंकि यहाँ आने जाने का कोई साधन ही नहीं था।
जब कोसी प्रोजेक्ट का काम शुरू हुआ तब टी.पी. सिंह ICS प्रशासक थे और पी.एन. शर्मा उप-प्रशासक थे। फिर लोग यहाँ आना-जाना शुरू हुए और उनके लिए राशन-पानी तथा रोजमर्रा की चीजों की जरूरत पड़ी। तब यह हुआ कि उस दुकान के लिए सामान कहाँ से आयेगा। सामान लाने की एक ही जगह थी और वह थी पूर्णिया। पूर्णिया से अगर सामान आयेगा तो वह केवल बथनाहा तक आ सकता था। उसे बीरपुर तक लाने की समस्या अभी भी बाकी रह जाती थी। तय हुआ कि बथनाहा से बीरपुर तक ट्रक से सामान आयेगा और पी.एन. शर्मा ने मेरे चाचा को जिम्मा दिया कि वह इसकी व्यवस्था करें। उन्होंने मुझसे कहा तो मैं रेलवे की ट्रैक पर सामान के साथ ट्रक लेकर अररिया तक आता था। अररिया के बाद यहाँ तक रास्ता कच्चा ही था। यहाँ अकाल था पर आबादी भी खास नहीं थी, इसलिये उतनी कोई समस्या भी नहीं थी। जो कुछ भी यहाँ है वह सब कोसी प्रोजेक्ट शुरू होने के बाद का है। उसके पहले यहाँ उस वक्त के जो भी लोग थे उनका जीवन आदिमानव जैसा था। जो भी मोटा कपड़ा मिला वह पहन लिया और जो भी मिला उसे खा कर जिंदगी बसर कर ली।
पिताजी द्वारा बीरपुर में जमीन खरीदने के बाद मेरा यहाँ आना-जाना शुरू हुआ। लेकिन यहाँ रहने के लिये मैं 1955 में आया जब पिताजी ने मुझे यहाँ भेजा। तब तक मैं पटोरी में अपनी दवा की दुकान पर बैठता था। हम लोगों को फारबिसगंज से बीरपुर तक का बस का परमिट मिल गया था। उस समय यहाँ एक मिठाई साह की चूड़ा-मूढ़ी की दुकान हुआ करती थी और अभी जहाँ एयरपोर्ट है उसके बगल में शालीमार कालोनी हुआ करती थी जो फूस से निर्मित थी। दिन में वहाँ कोई कुछ नहीं खाता था क्योंकि जब हवा चलती थी तब बालू उड़ कर थाली में आ जाता था। रात में हवा शान्त रहती थी। एक बार उस कालोनी में आग लग गयी तब उस घटना के बाद यह नयी वाली कालोनी बनी।